देह- भाव से यहाँ कोई भी अपना नहीं है , परमात्म-भाव से सभी अपने हैं ।
हमारे जीवन में गर्भाधान से लेकर श्मशान तक , या कहें तो लोक - लोकांतर तक यह सत्य हमारे आचार और विचार को अनुशासित करता रहा है । वर्ण और आश्रम का आधार भी यही है -- समाज का विकास वर्ण द्वारा और व्यक्ति का विकास आश्रम द्वारा । ब्राह्मण, क्षत्रिय , वैश्य , शूद्र -- गुण और कर्मों के आधार पर ही हुवा और ब्रह्मचारी , गृहस्थ , वानप्रस्थ और संन्यास भी व्यक्ति के विकास - क्रम के परिसूचक हैं । सभी वर्णों और सभी आश्रमों का समाज के प्रति , देश के प्रति एवं विश्व के प्रति दायित्व है , जिसे पूरा करने में ही उसकी वास्तविकता तथा सार्थकता सिद्ध होती है ।
उसमें कोई बड़ा अथवा छोटा नहीं है । सबकी अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका है । इसी प्रकार चतुर्वर्ग भी हैं -- धर्म , अर्थ ,काम और मोक्ष । इसमें धर्म द्वारा अनुमोदित अर्थ हो तथा मोक्ष की ओर उन्मुख काम का भाव होना चाहिए । इसमें अर्थ को धर्म, काम को मोक्ष अनुशासित करता है । इन चारों से परे ऋषियों ने प्रेम को भी पंचम पुरुषार्थ स्वीकार किया है , जो अपने आप में परम ओर चरम है। यदि चतुर्वर्ग को ही ध्यान से देखा जाये तो स्पष्ट है कि आर्य - जीवन में लोक- जीवन की कभी भी उपेक्षा नहीं की गयी है , प्रत्युत उसकी पूर्ण स्वीकृति है ।
जिसका लोक सफल नहीं है , उसका परलोक भी असफल ही है । जिसने लोक की उपेक्षा की उसका परलोक स्वयं उपेक्षित हो गया । क्योंकि ' जगत मिथ्या ' चिल्लाने से कुछ होता नहीं ; यह सम्पूर्ण जगत स्वयं परब्रह्म परमात्मा का दिव्य मंगलमय स्वरूप है । साथ ही यह शरीर भी तो उसी ईश्वर का मंदिर है ; मंदिर की उपेक्षा होने से उसमें निवास करने वाले देवता का निरादर हो जाता है । परिणामत: यहाँ कुछ भी उपेक्षा के योग्य नहीं है -- ' there is nothing unholy on this earth for GOD'S feet are everywhere। '
आर्यों ने इस परम सत्य को स्वीकार किया परिणामत: उनका लौकिक जीवन भी कर्म ओर सौंदर्य से पूरित है । सम्पूर्ण उदात्त गुणों का समन्वित रूप ही आर्य है । यहाँ जीवन की विविधता में एक समस्वरता ओर समरसता की वीणा झंकृत होती रही है । यहाँ कर्म , भक्ति और ज्ञान में कोई उपेक्षित नहीं है । बल है कर्म , परन्तु इसमें भक्ति का रस ओर ज्ञान की ज्योति सदैव जागृत है । कर्म के भीतर से ही भक्ति और ज्ञान भी ज्योतित हैं । आर्य कभी भी किसी भी दिशा में चिंतित , खिन्न , अवसन्न , जढ़ , मूर्छित , किंकर्त्तव्य - विमूढ़ नहीं होगा । वह सदा सदैव हर हालत में निर्भय एवं भय रहित रहेगा । प्रसन्नता उसमें बनी रहेगी । ये सभी गुण उसमें सहज- स्वाभाविक रूप से बने रहेंगे । इनके लिए उसे कोई विशिष्ट साधना का उपक्रम नहीं करना पड़ेगा ।
वह आर्य -- " अभयं नक्तमभयम दिवा: न: सर्वा: आशा मम मित्रं भवन्तु " जो सभी प्राणियों को अपने भीतर देखता है और सब प्राणियों में अपने को पाता है , वह किसी प्रकार के संशय से ग्रस्त नहीं रहता । इस एकत्व बोध में समस्वरता और सामरस्य की आधारशिला समन्वय की भावना ही है। यह श्रेय और प्रेय में , लोक और परलोक में , स्व और पर में , ऋत और सत्य में , जीव और ब्रह्म में , प्रत्यक्ष और परोक्ष में , व्यक्ति और समाज में , जड़ और चेतन में आदि में समान रूप से अनुस्यूत है । देह- भाव से यहाँ कोई भी अपना नहीं है , परमात्म-भाव से सभी अपने हैं ।**********************
हमारे जीवन में गर्भाधान से लेकर श्मशान तक , या कहें तो लोक - लोकांतर तक यह सत्य हमारे आचार और विचार को अनुशासित करता रहा है । वर्ण और आश्रम का आधार भी यही है -- समाज का विकास वर्ण द्वारा और व्यक्ति का विकास आश्रम द्वारा । ब्राह्मण, क्षत्रिय , वैश्य , शूद्र -- गुण और कर्मों के आधार पर ही हुवा और ब्रह्मचारी , गृहस्थ , वानप्रस्थ और संन्यास भी व्यक्ति के विकास - क्रम के परिसूचक हैं । सभी वर्णों और सभी आश्रमों का समाज के प्रति , देश के प्रति एवं विश्व के प्रति दायित्व है , जिसे पूरा करने में ही उसकी वास्तविकता तथा सार्थकता सिद्ध होती है ।
उसमें कोई बड़ा अथवा छोटा नहीं है । सबकी अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका है । इसी प्रकार चतुर्वर्ग भी हैं -- धर्म , अर्थ ,काम और मोक्ष । इसमें धर्म द्वारा अनुमोदित अर्थ हो तथा मोक्ष की ओर उन्मुख काम का भाव होना चाहिए । इसमें अर्थ को धर्म, काम को मोक्ष अनुशासित करता है । इन चारों से परे ऋषियों ने प्रेम को भी पंचम पुरुषार्थ स्वीकार किया है , जो अपने आप में परम ओर चरम है। यदि चतुर्वर्ग को ही ध्यान से देखा जाये तो स्पष्ट है कि आर्य - जीवन में लोक- जीवन की कभी भी उपेक्षा नहीं की गयी है , प्रत्युत उसकी पूर्ण स्वीकृति है ।
जिसका लोक सफल नहीं है , उसका परलोक भी असफल ही है । जिसने लोक की उपेक्षा की उसका परलोक स्वयं उपेक्षित हो गया । क्योंकि ' जगत मिथ्या ' चिल्लाने से कुछ होता नहीं ; यह सम्पूर्ण जगत स्वयं परब्रह्म परमात्मा का दिव्य मंगलमय स्वरूप है । साथ ही यह शरीर भी तो उसी ईश्वर का मंदिर है ; मंदिर की उपेक्षा होने से उसमें निवास करने वाले देवता का निरादर हो जाता है । परिणामत: यहाँ कुछ भी उपेक्षा के योग्य नहीं है -- ' there is nothing unholy on this earth for GOD'S feet are everywhere। '
आर्यों ने इस परम सत्य को स्वीकार किया परिणामत: उनका लौकिक जीवन भी कर्म ओर सौंदर्य से पूरित है । सम्पूर्ण उदात्त गुणों का समन्वित रूप ही आर्य है । यहाँ जीवन की विविधता में एक समस्वरता ओर समरसता की वीणा झंकृत होती रही है । यहाँ कर्म , भक्ति और ज्ञान में कोई उपेक्षित नहीं है । बल है कर्म , परन्तु इसमें भक्ति का रस ओर ज्ञान की ज्योति सदैव जागृत है । कर्म के भीतर से ही भक्ति और ज्ञान भी ज्योतित हैं । आर्य कभी भी किसी भी दिशा में चिंतित , खिन्न , अवसन्न , जढ़ , मूर्छित , किंकर्त्तव्य - विमूढ़ नहीं होगा । वह सदा सदैव हर हालत में निर्भय एवं भय रहित रहेगा । प्रसन्नता उसमें बनी रहेगी । ये सभी गुण उसमें सहज- स्वाभाविक रूप से बने रहेंगे । इनके लिए उसे कोई विशिष्ट साधना का उपक्रम नहीं करना पड़ेगा ।
वह आर्य -- " अभयं नक्तमभयम दिवा: न: सर्वा: आशा मम मित्रं भवन्तु " जो सभी प्राणियों को अपने भीतर देखता है और सब प्राणियों में अपने को पाता है , वह किसी प्रकार के संशय से ग्रस्त नहीं रहता । इस एकत्व बोध में समस्वरता और सामरस्य की आधारशिला समन्वय की भावना ही है। यह श्रेय और प्रेय में , लोक और परलोक में , स्व और पर में , ऋत और सत्य में , जीव और ब्रह्म में , प्रत्यक्ष और परोक्ष में , व्यक्ति और समाज में , जड़ और चेतन में आदि में समान रूप से अनुस्यूत है । देह- भाव से यहाँ कोई भी अपना नहीं है , परमात्म-भाव से सभी अपने हैं ।**********************













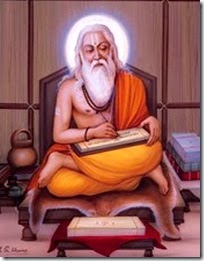




कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें